राजस्थान भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित एक विशाल राज्य है, जिसकी जलवायु इसकी भौगोलिक स्थिति, अरावली पर्वतमाला की स्थिति और थार रेगिस्तान की उपस्थिति से अत्यधिक प्रभावित होती है। राज्य की जलवायु में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, जहाँ एक ओर पश्चिमी भाग में अत्यधिक शुष्क दशाएँ मिलती हैं, वहीं दक्षिणी-पूर्वी भाग में आर्द्र दशाएँ भी देखने को मिलती हैं। राजस्थान की जलवायु को समझना राज्य के कृषि पैटर्न, जल संसाधनों और जनजीवन पर इसके प्रभाव को जानने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
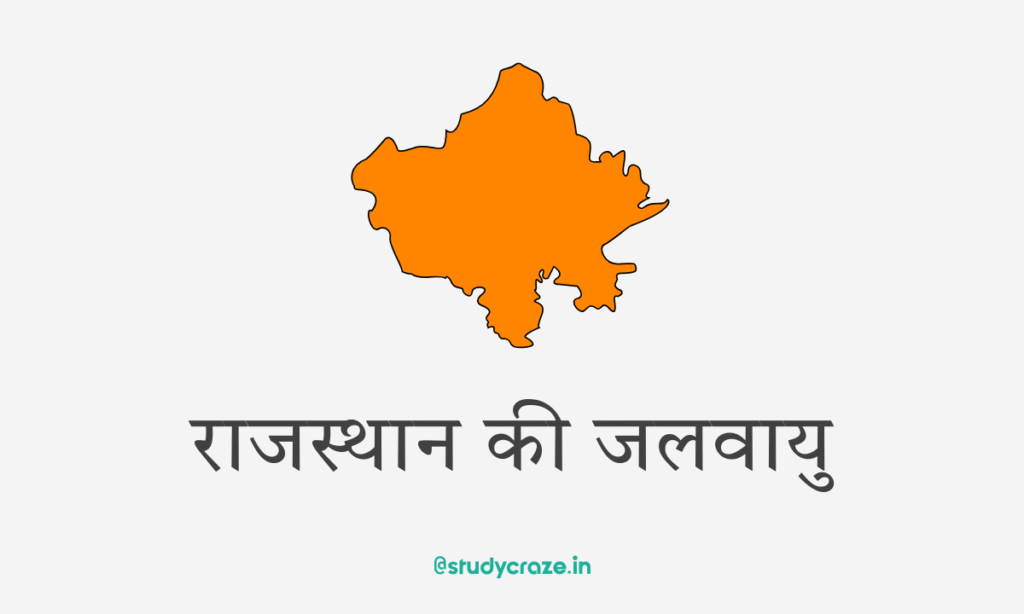
1. जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक
राजस्थान की जलवायु को मुख्य रूप से निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं:
- अक्षांशीय स्थिति: राजस्थान का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। कर्क रेखा (23∘30′ उत्तरी अक्षांश) राज्य के दक्षिणी भाग (बांसवाड़ा जिले के मध्य से) से गुजरती है, जिसके कारण दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रभाव अधिक होता है।
- समुद्र से दूरी: राजस्थान की समुद्र तट से अधिक दूरी (लगभग 300 किमी से अधिक) होने के कारण यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, जिसमें दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक होता है।
- अरावली पर्वतमाला की स्थिति: अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो असमान भागों में विभाजित करती है। इसकी दिशा (दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व) मानसूनी हवाओं के समानांतर होने के कारण ये हवाएँ बिना रुकावट के निकल जाती हैं, जिससे पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है। यह एक महत्वपूर्ण जल विभाजक के रूप में भी कार्य करती है।
- थार का मरुस्थल: पश्चिमी राजस्थान में विशाल थार मरुस्थल की उपस्थिति तापमान को बहुत अधिक बढ़ा देती है, जिससे ग्रीष्मकाल में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, जो मानसून को आकर्षित करता है। साथ ही, रेत की तीव्र तापन और शीतलन क्षमता के कारण यहाँ दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है।
- वनस्पति का अभाव: पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति आवरण की कमी भी उच्च तापमान और कम वर्षा का एक कारण है, क्योंकि वनस्पति वाष्पोत्सर्जन और वर्षा को प्रभावित करती है।
- धूल भरी आँधियाँ और गर्म हवाएँ (लू): ग्रीष्मकाल में चलने वाली धूल भरी आँधियाँ और ‘लू’ (गर्म हवाएँ) यहाँ के तापमान को और बढ़ा देती हैं, जिससे जलवायु शुष्क और असहज हो जाती है।
2. राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण
राजस्थान की जलवायु को मोटे तौर पर पाँच प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
2.1. शुष्क जलवायु प्रदेश (Dry Climate Region)
- विस्तार: जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलौदी और पश्चिमी जोधपुर का अधिकांश भाग।
- विशेषताएँ:
- वर्षा: 0 से 20 सेमी प्रति वर्ष।
- तापमान: ग्रीष्मकाल में अत्यधिक गर्म (कभी-कभी 50∘C से अधिक), शीतकाल में भी ठंडी रातें।
- वनस्पति: नगण्य, केवल कँटीली झाड़ियाँ और मरुस्थलीय घास।
- मिट्टी: रेतीली, बलुई।
- कारण: अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होना, समुद्र से अधिक दूरी और थार मरुस्थल का प्रभाव।
- प्रमुख घटनाएँ: गर्मियों में धूल भरी आँधियाँ और लू का चलना।
2.2. अर्द्ध-शुष्क जलवायु प्रदेश (Semi-Arid Climate Region)
- विस्तार: चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर का पूर्वी भाग, जोधपुर का पूर्वी भाग, डीडवाना-कुचामन, बालोतरा, ब्यावर, सांचौर, डीडवाना।
- विशेषताएँ:
- वर्षा: 20 से 40 सेमी प्रति वर्ष।
- तापमान: ग्रीष्मकाल में उच्च, शीतकाल में मध्यम ठंडी।
- वनस्पति: स्टेपी प्रकार की वनस्पति, घास और कँटीली झाड़ियाँ।
- मिट्टी: रेतीली-दोमट।
- कारण: यह शुष्क प्रदेश और अरावली के बीच का संक्रमण क्षेत्र है।
- कृषि: बाजरा, दलहन जैसी शुष्क कृषि फसलें उगाई जाती हैं।
2.3. उप-आर्द्र जलवायु प्रदेश (Sub-Humid Climate Region)
- विस्तार: जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, अलवर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, सीकर, कोटा का पश्चिमी भाग, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा।
- विशेषताएँ:
- वर्षा: 40 से 60 सेमी प्रति वर्ष।
- तापमान: ग्रीष्मकाल में गर्म, शीतकाल में ठंडा।
- वनस्पति: मिश्रित पतझड़ वनस्पति और घास के मैदान।
- मिट्टी: जलोढ़ और लाल-पीली मिट्टी।
- कारण: अरावली के पूर्वी ढलान पर स्थित होना, जिससे मानसूनी हवाओं से कुछ वर्षा प्राप्त होती है।
2.4. आर्द्र जलवायु प्रदेश (Humid Climate Region)
- विस्तार: भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डीग, गंगापुर सिटी।
- विशेषताएँ:
- वर्षा: 60 से 80 सेमी प्रति वर्ष।
- तापमान: ग्रीष्मकाल में अपेक्षाकृत कम गर्म, शीतकाल में सामान्य ठंडा।
- वनस्पति: सघन पतझड़ वनस्पति।
- मिट्टी: काली और लाल-लोमी मिट्टी।
- कारण: मानसूनी हवाओं से अधिक वर्षा प्राप्त होना।
- कृषि: गेहूं, चना, सरसों, मक्का जैसी फसलें।
2.5. अति-आर्द्र जलवायु प्रदेश (Very Humid Climate Region)
- विस्तार: दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान, जिसमें बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू (सिरोही) का कुछ भाग शामिल है।
- विशेषताएँ:
- वर्षा: 80 से 150 सेमी प्रति वर्ष (माउंट आबू में सर्वाधिक, 150 सेमी से अधिक)।
- तापमान: ग्रीष्मकाल में सामान्य, शीतकाल में सुहावना।
- वनस्पति: सघन सदाबहार और मानसूनी वन।
- मिट्टी: लाल-काली मिट्टी।
- कारण: बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त होना, तथा पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा का अधिक होना।
- सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान: माउंट आबू (150 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा)।
- सर्वाधिक वर्षा वाला जिला: झालावाड़ (लगभग 100 सेमी औसत वार्षिक वर्षा)।
3. ऋतुएँ (Seasons)
राजस्थान में मुख्य रूप से तीन प्रमुख ऋतुएँ पाई जाती हैं:
3.1. ग्रीष्म ऋतु (Summer Season) – मार्च से मध्य जून
- विशेषताएँ:
- उच्च तापमान: मार्च के बाद तापमान तेजी से बढ़ता है और मई-जून में यह अपने चरम पर होता है। पश्चिमी राजस्थान में 45∘C से 50∘C तक तापमान दर्ज किया जाता है।
- निम्न वायुदाब: अत्यधिक गर्मी के कारण वायुदाब कम हो जाता है।
- आँधियाँ: मई-जून में धूल भरी आँधियाँ चलना सामान्य बात है, खासकर पश्चिमी राजस्थान में। श्री गंगानगर में सर्वाधिक आँधियाँ आती हैं।
- लू: शुष्क और गर्म स्थानीय हवाएँ, जिन्हें ‘लू’ कहा जाता है, चलती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं।
3.2. वर्षा ऋतु (Monsoon Season) – मध्य जून से सितंबर
- विशेषताएँ:
- मानसून का आगमन: राजस्थान में मानसून का आगमन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से होता है।
- अरब सागर का मानसून: यह राजस्थान में दक्षिण-पश्चिमी दिशा से प्रवेश करता है, खासकर बांसवाड़ा जिले से। यह अरावली के समानांतर होने के कारण पश्चिमी राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं कर पाता, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में अच्छी वर्षा करता है।
- बंगाल की खाड़ी का मानसून: यह पूर्वी राजस्थान में उत्तर-पूर्वी दिशा से प्रवेश करता है। यह पूर्वी और दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा करता है।
- वर्षा का वितरण: राजस्थान में वर्षा का वितरण असमान है। पश्चिमी भागों में बहुत कम वर्षा होती है, जबकि दक्षिणी-पूर्वी भागों में अधिक वर्षा होती है।
- अकाल और सूखा: अपर्याप्त और अनियमित वर्षा के कारण राजस्थान में अक्सर अकाल और सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है।
- मानसून प्रत्यावर्तन (लौटता मानसून): सितंबर के अंत में मानसून लौटने लगता है, जिससे तापमान फिर से बढ़ने लगता है।
- मानसून का आगमन: राजस्थान में मानसून का आगमन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से होता है।
3.3. शीत ऋतु (Winter Season) – अक्टूबर से फरवरी
- विशेषताएँ:
- तापमान में गिरावट: अक्टूबर से तापमान गिरना शुरू हो जाता है।
- मावठ: शीतकाल में भूमध्यसागरीय पश्चिमी विक्षोभों (Western Disturbances) के कारण होने वाली वर्षा को ‘मावठ’ कहते हैं। यह वर्षा रबी की फसलों (जैसे गेहूं, जौ, चना) के लिए अत्यंत लाभदायक होती है, जिसे ‘गोल्डन ड्रॉप्स’ भी कहा जाता है।
- शीतलहर: उत्तरी भारत से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में तीव्र शीतलहर चलती है।
- पाला: कभी-कभी अत्यधिक ठंड के कारण पाला भी पड़ता है, जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है।
- तापमान: दिसंबर-जनवरी में तापमान काफी गिर जाता है, चूरू जैसे स्थानों पर 0∘C से नीचे भी जा सकता है।
4. कोपेन का जलवायु वर्गीकरण (Koppen’s Climate Classification)
कोपेन ने वनस्पति, तापमान और वर्षा के आधार पर राजस्थान की जलवायु को चार प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया है, जो अधिक वैज्ञानिक और व्यापक रूप से स्वीकार्य है:
- BWhw (शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु):
- विस्तार: पश्चिमी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, फलौदी, अनूपगढ़।
- विशेषताएँ: बहुत कम वर्षा, अत्यधिक उच्च तापमान, शुष्क परिस्थितियाँ, नगण्य वनस्पति। ‘h’ का अर्थ गर्म और शुष्क, ‘w’ का अर्थ शीतकाल शुष्क।
- प्रतिनिधि जिले: जैसलमेर, बीकानेर।
- BSwhw (अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु):
- विस्तार: चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर का पूर्वी भाग, जोधपुर का पूर्वी भाग, डीडवाना-कुचामन, बालोतरा, ब्यावर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़।
- विशेषताएँ: 20−40 सेमी वर्षा, ग्रीष्मकाल में गर्म, शीतकाल में ठंडा, स्टेपी प्रकार की वनस्पति। ‘S’ का अर्थ स्टेपी।
- प्रतिनिधि जिले: नागौर, सीकर।
- Cwg (उप-आर्द्र मानसूनी जलवायु):
- विस्तार: अरावली के पूर्वी भाग से सटे जिले जैसे जयपुर, दौसा, अलवर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डीग, गंगापुर सिटी।
- विशेषताएँ: 40−60 सेमी वर्षा, शीतकाल शुष्क, मानसूनी वर्षा ग्रीष्मकाल में। ‘g’ का अर्थ गंगा का मैदान।
- प्रतिनिधि जिले: जयपुर, अजमेर।
- Aw (उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु):
- विस्तार: दक्षिणी राजस्थान, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, दक्षिणी चित्तौड़गढ़ और माउंट आबू क्षेत्र शामिल है।
- विशेषताएँ: 80−150 सेमी वर्षा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार या मानसूनी वन, वर्षभर उच्च तापमान (शीतकाल में भी न्यूनतम नहीं)। ‘A’ का अर्थ उष्णकटिबंधीय आर्द्र, ‘w’ का अर्थ शीतकाल शुष्क।
- प्रतिनिधि जिले: बांसवाड़ा, झालावाड़।
5. थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण (Thornthwaite’s Climate Classification)
थॉर्नवेट का वर्गीकरण वर्षा की प्रभावशीलता और तापीय दक्षता पर आधारित है:
- EA’d (शुष्क मरुस्थलीय जलवायु):
- विस्तार: पश्चिमी राजस्थान (जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर का अधिकांश भाग)।
- विशेषताएँ: अत्यधिक शुष्क।
- DB’w (अर्द्ध-शुष्क जलवायु):
- विस्तार: मध्य राजस्थान (जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर)।
- विशेषताएँ: वर्षा की कुछ कमी।
- CA’w (उप-आर्द्र जलवायु):
- विस्तार: पूर्वी राजस्थान (जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर)।
- विशेषताएँ: पर्याप्त वर्षा।
- DA’w (आर्द्र जलवायु):
- विस्तार: दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान (कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा)।
- विशेषताएँ: अधिक वर्षा।
6. ट्रेवार्थ का जलवायु वर्गीकरण (Trewartha’s Climate Classification)
ट्रेवार्थ का वर्गीकरण भी कोपेन के समान है, लेकिन इसमें कुछ भिन्नताएँ हैं:
- BW (मरुस्थलीय जलवायु):
- विस्तार: पश्चिमी राजस्थान (जैसलमेर, बीकानेर)।
- BS (स्टेपी जलवायु):
- विस्तार: अर्द्ध-शुष्क प्रदेश।
- Aw (उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु):
- विस्तार: दक्षिणी राजस्थान (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़)।
- CAw (उप-आर्द्र जलवायु):
- विस्तार: पूर्वी राजस्थान।
7. जलवायु परिवर्तन और चुनौतियाँ
हाल के वर्षों में राजस्थान में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे जा रहे हैं:
- अनियमित वर्षा पैटर्न: वर्षा की मात्रा और समय में अनिश्चितता बढ़ी है, जिससे कभी बाढ़ तो कभी सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है।
- तापमान में वृद्धि: औसत तापमान में वृद्धि हुई है, जिससे ग्रीष्मकाल अधिक गर्म और लंबा होता जा रहा है।
- जल संकट: भूजल स्तर में गिरावट और जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा है।
- मरुस्थलीकरण का विस्तार: पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीकरण की समस्या गंभीर होती जा रही है, जिससे उपजाऊ भूमि भी प्रभावित हो रही है।
- कृषि पर प्रभाव: वर्षा आधारित कृषि अत्यधिक प्रभावित हो रही है, जिससे किसानों की आजीविका पर असर पड़ रहा है।
इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जल संरक्षण, वनारोपण, सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग और जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाना आवश्यक है।
8. राजस्थान में वर्षा के वितरण के प्रमुख कारण
- अरावली पर्वतमाला की स्थिति: जैसा कि ऊपर बताया गया है, अरावली की दिशा मानसूनी हवाओं के समानांतर होने के कारण वे बिना वर्षा किए गुजर जाती हैं।
- थार मरुस्थल की भूमिका: थार मरुस्थल उच्च तापमान के कारण निम्न वायुदाब क्षेत्र बनाता है, जो मानसून को आकर्षित करता है, लेकिन स्वयं शुष्क रहने के कारण नमी कम छोड़ता है।
- बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शाखाएँ: बंगाल की खाड़ी का मानसून पूर्वी और दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान में वर्षा करता है, जबकि अरब सागर का मानसून दक्षिणी राजस्थान तक ही सीमित रहता है।
निष्कर्ष
राजस्थान की जलवायु एक जटिल और विविध प्रणाली है जो राज्य के भूगोल और जीवन शैली को गहराई से प्रभावित करती है। शुष्क पश्चिमी मरुस्थल से लेकर दक्षिणी-पूर्वी के अति-आर्द्र क्षेत्रों तक, राजस्थान विभिन्न प्रकार की जलवायु परिस्थितियों को समेटे हुए है। राज्य की विकास योजनाओं और भविष्य की रणनीतियों के लिए इसकी जलवायु को समझना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अध्याय राजस्थान की जलवायु के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जो छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगी।
